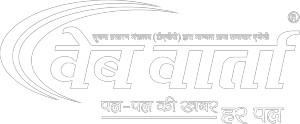-प्रियंका सौरभ-
देश की न्याय व्यवस्था कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों से जूझ रही है, जिसका मुख्य कारण भारतीय अदालतों में अभी भी 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। यह लंबित मामले न केवल न्याय में देरी करते हैं, बल्कि कानूनी व्यवस्था में लोगों का भरोसा भी कम करते हैं। इनमें से कई मामले एक दशक से अधिक समय से लंबित हैं, जिनमें से लगभग 50 लाख मामले दस साल से भी अधिक समय पहले शुरू किए गए थे। नीति आयोग ने सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया है, चेतावनी दी है कि मामले के समाधान की वर्तमान गति से, केवल निचली अदालतों में लंबित मामलों को हल करने में 300 साल से अधिक लग सकते हैं। भारत में, “लंबित मामलों” का अर्थ कानूनी ढांचे के भीतर अनसुलझे मामलों की भारी संख्या है। स्थिति विशेष रूप से निचले न्यायिक स्तरों पर गंभीर है, जहाँ अधिकांश मामले दायर किए जाते हैं और न्यायाधीशों की कमी से निपटान नहीं होता है। लंबित मामलों की बढ़ती संख्या भारतीय न्याय वितरण प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती है।
लंबी कानूनी प्रक्रियाएँ “न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है” कहावत को चरितार्थ करती हैं, क्योंकि वे जनता के विश्वास को ख़त्म करती हैं और व्यक्तियों को समय पर न्याय से वंचित करती हैं। बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद जैसे मामलों के लंबे समाधान ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ दिया है, जिसमें लगभग 70 साल लग गए। अदालतों में मामलों की विशाल मात्रा अदालती दक्षता में बाधा डालती है और लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि करती है, जिससे त्वरित न्याय लगभग असंभव हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में 82, 000 से अधिक और उच्च न्यायालयों में 62 लाख से अधिक मामले लंबित होने के कारण, निर्णयों में बड़ी देरी आम बात है। मुकदमेबाजी का वित्तीय बोझ आर्थिक विकास को भी बाधित करता है, क्योंकि यह संसाधनों को ख़त्म करता है और व्यक्तियों और व्यवसायों को कानूनी कार्यवाही करने से हतोत्साहित करता है। भारत में न्यायिक देरी की अनुमानित लागत दो मिलियन डॉलर से अधिक है। न्याय प्रणाली पर लंबित मामलों का प्रभाव गहरा और दूरगामी है। लंबे समय तक चलने वाले मामले कानूनी प्रणाली में जनता के विश्वास को ख़त्म कर सकते हैं, जिससे इसकी प्रभावशीलता के बारे में निराशा और संदेह पैदा होता है, जिससे कुछ लोग वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों की तलाश करने लगते हैं। देरी का यह चक्र समस्या को और बढ़ाता है।
न्यायिक देरी में योगदान देने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारक जनसंख्या के लिए न्यायाधीशों का अपर्याप्त अनुपात है। भारत में, विकसित देशों की तुलना में कानूनी प्रणाली बहुत धीमी गति से काम करती है, जहाँ हर दस लाख निवासियों के लिए केवल 21 न्यायाधीश उपलब्ध हैं। सरकार सबसे बड़ी वादी है, जो सभी लंबित मामलों में से लगभग आधे मामलों के लिए ज़िम्मेदार है, जिनमें से कई तुच्छ मुद्दों पर अपील में बंधे हैं। सीमित कोर्ट रूम स्पेस और पुरानी केस मैनेजमेंट प्रथाओं जैसी चुनौतियों से लंबी अदालती कार्यवाही और भी जटिल हो जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र ने 15 वर्षों में 200, 000 से अधिक मामलों को सफलतापूर्वक हल किया है, जो वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों की प्रभावशीलता को उजागर करता है। दुर्भाग्य से, वकील और वादी दोनों अक्सर स्थगन का दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण मामले सालों या दशकों तक टल जाते हैं।
मैन्युअल दस्तावेज़ीकरण और पुरानी कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भरता मामलों के समय पर समाधान में बाधा डालती है, जिससे अनावश्यक नौकरशाही बाधाएँ पैदा होती हैं। लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने के लिए, यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि कार्यवाही निरंतर हो। इसमें बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए न्यायालय स्टाफिंग और बुनियादी ढांचे में निवेश करना शामिल है। न्यायालयों की संख्या बढ़ाने और पर्याप्त सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करने से प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिल सकती है। मामलों को अधिक तेज़ी से ट्रैक करने और आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी केस प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना भी महत्त्वपूर्ण है। उचित रूप से प्रबंधित मामलों के समय पर समाधान तक पहुँचने की अधिक संभावना होती है। कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कानूनों की नियमित समीक्षा और संशोधन अनिश्चितता को कम करने और कानूनी कार्यवाही में तेजी लाने के लिए आवश्यक है।
वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान की सुविधा के लिए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 स्थगन पर सख्त नियम लागू करता है। मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता को अनिवार्य करके वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने से अदालतों पर बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। मध्यस्थता अधिनियम (2023) वाणिज्यिक और नागरिक विवादों में मध्यस्थता को अनिवार्य बनाकर इसका समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य अदालती लंबित मामलों को कम करना है। एक मज़बूत लोकतंत्र न्याय के त्वरित और प्रभावी वितरण पर निर्भर करता है। न्यायिक देरी से निपटने के लिए, न्यायिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, मौजूदा रिक्तियों को भरना, ऐआई-संचालित केस प्रबंधन को अपनाना और वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देना आवश्यक है। न्यायिक जवाबदेही को दूरदर्शी नीति ढांचे के साथ जोड़कर, भारत की न्याय प्रणाली अधिक निष्पक्ष, सुलभ और समय पर बन सकती है। यह आशा की जाती है कि सभी हितधारक-न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, सरकारें और कानूनी पेशेवर-न्याय वितरण प्रणाली को मज़बूत करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे। भारतीय अदालतों में लंबित मामलों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें तकनीकी प्रगति के साथ-साथ प्रशासनिक, कानूनी और बुनियादी ढाँचे में सुधार शामिल हो। हालाँकि प्रगति हुई है, लेकिन कानूनी प्रणाली में विश्वास बहाल करने और विवादों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास महत्त्वपूर्ण हैं। भारतीय न्यायपालिका मूल कारणों से निपट सकती है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिनव समाधान लागू कर सकती है।