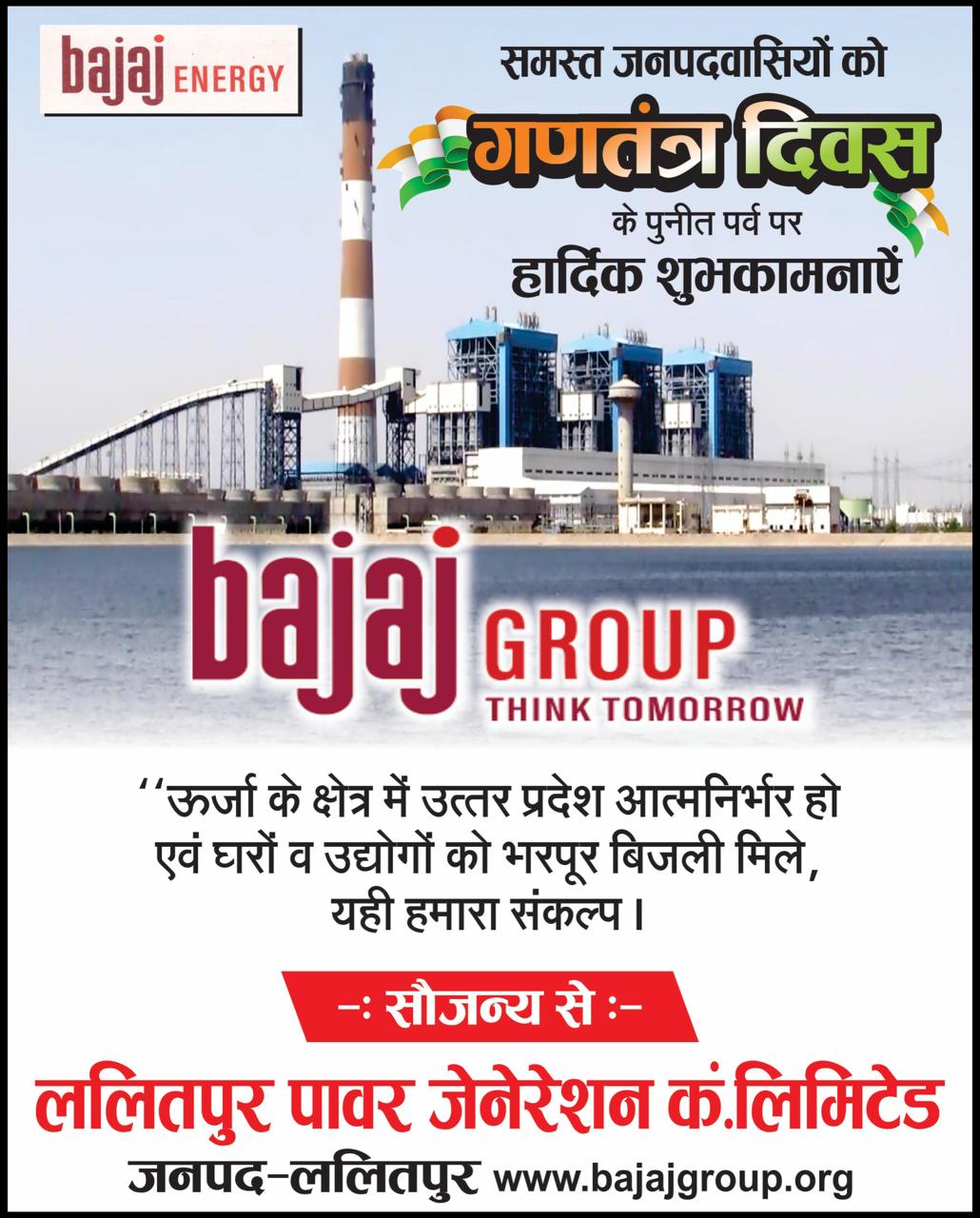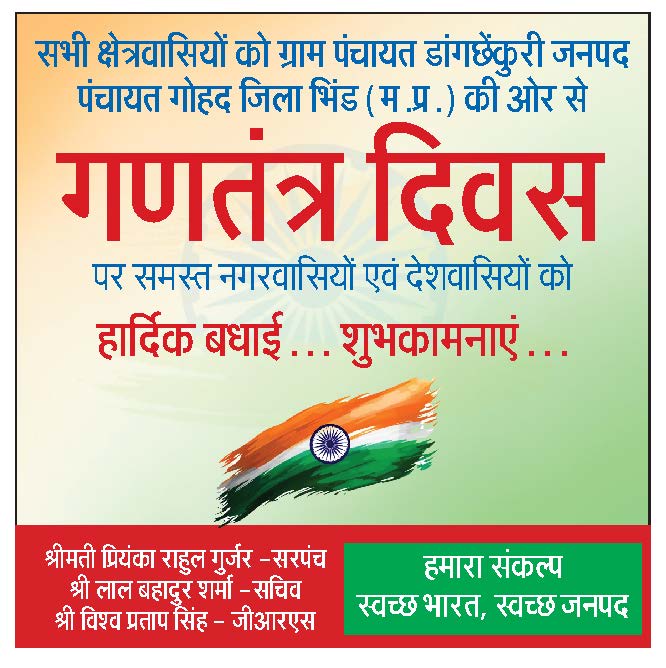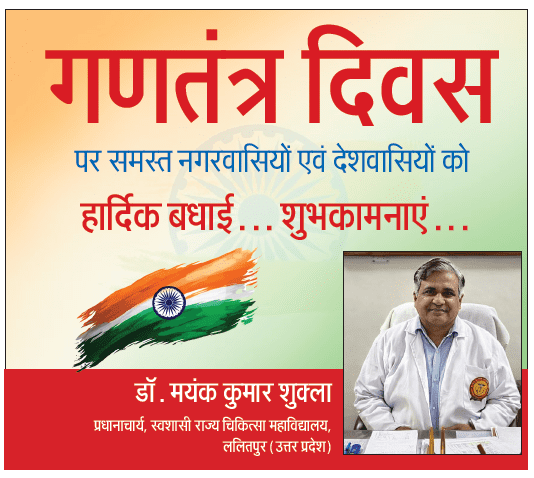-डॉ. शैलेश शुक्ला-
भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां तकनीकी प्रगति अपने चरम पर है। डिजिटल भारत का सपना अब केवल एक सरकारी नारा नहीं, बल्कि आम नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा बन चुका है। स्मार्टफोन, इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट्स और सोशल मीडिया का विस्तार इतना व्यापक हो चुका है कि देश की एक बड़ी आबादी अब हर क्षण डिजिटल रूप से जुड़ी रहती है। लेकिन इस डिजिटल विकास की चमक के पीछे एक गंभीर खतरा भी छिपा है — नागरिकों की निजता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा। हर बार जब कोई उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट पर लॉगिन करता है, किसी ऐप को डाउनलोड करता है या सोशल मीडिया पर कोई जानकारी साझा करता है, तब वह जाने-अनजाने में अपना निजी डेटा विभिन्न कंपनियों और संस्थाओं को सौंप रहा होता है। यह डेटा न केवल उनकी पहचान, स्थान और आदतों से जुड़ा होता है, बल्कि कई बार उनकी संवेदनशील जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स और पर्सनल कॉन्वर्सेशन तक को शामिल करता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या आम नागरिक को पता है कि उसका डेटा कहां जा रहा है, किसके पास जमा हो रहा है और उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है?
भारतीय संदर्भ में निजता का अधिकार लंबे समय तक एक अस्पष्ट विचार रहा। लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने इसे मौलिक अधिकार घोषित कर एक नई दिशा दी। अदालत ने कहा कि निजता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है। यह निर्णय उस समय आया जब आधार जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार बड़े पैमाने पर नागरिकों की जानकारी एकत्र कर रही थी। हालांकि, यह फैसला अपने-आप में एक बड़ी जीत था, पर यह स्पष्ट था कि केवल एक न्यायिक घोषणा से डिजिटल निजता की रक्षा नहीं हो सकती। भारत को एक स्पष्ट, सख्त और व्यावहारिक डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकता थी जो कंपनियों और सरकारी एजेंसियों दोनों को जवाबदेह बना सके। खासकर ऐसे समय में जब तकनीकी कंपनियां उपयोगकर्ताओं की जानकारी को बिना उनकी सहमति के इस्तेमाल कर विज्ञापनों, सिफारिशों और विश्लेषणों के लिए बेच रही थीं। इसके अलावा साइबर अपराध, डेटा लीक और रैंसमवेयर अटैक जैसे खतरे भी निरंतर बढ़ते जा रहे थे।
यूरोप जैसे देशों में जहां जीडीपीआर (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन) जैसे कानून नागरिकों को उनके डेटा पर पूरा अधिकार देते हैं, भारत लंबे समय तक ऐसे किसी व्यापक कानून के अभाव में रहा। हालांकि 2000 में बना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कुछ हद तक साइबर अपराधों को नियंत्रित करता है, लेकिन यह कानून डेटा संग्रह, उपयोग, संरक्षण और सहमति के बारीक पहलुओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता। नतीजतन, टेक कंपनियों और यहां तक कि सरकारी एजेंसियों द्वारा भी बार-बार नागरिकों की निजता का उल्लंघन होता रहा। इसी को देखते हुए 2017 में B.N. श्रीकृष्णा समिति का गठन किया गया, जिसने 2018 में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में डेटा को नया तेल कहा गया और एक स्वतंत्र डेटा संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश की गई। यह समिति नागरिकों को उनके डेटा पर नियंत्रण देने और कंपनियों को जवाबदेह बनाने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचे की वकालत करती रही।
इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि 2023 में भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया। यह कानून न केवल भारत का पहला समर्पित डेटा संरक्षण कानून है, बल्कि यह देश में डिजिटल अधिकारों की नींव को सशक्त करता है। इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता है — उपयोगकर्ता की स्पष्ट सहमति। अब कोई भी संस्था, कंपनी या एजेंसी आपकी व्यक्तिगत जानकारी तभी एकत्र कर सकती है जब आप उसकी स्पष्ट अनुमति दें और वह अनुमति पारदर्शी भाषा में मांगी जानी चाहिए। साथ ही, उपयोगकर्ता को यह अधिकार भी प्राप्त होगा कि वह कभी भी अपनी सहमति वापस ले सके। इस कानून में एक स्वतंत्र डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की भी स्थापना की गई है जो कानून उल्लंघन के मामलों की जांच करेगा और दोषियों को दंडित करेगा। इसके अतिरिक्त, इस कानून के अंतर्गत डेटा उल्लंघन की स्थिति में कंपनियों को समय पर सूचना देना अनिवार्य बनाया गया है — जो अब तक भारतीय परिप्रेक्ष्य में अभूतपूर्व कदम है।
हालांकि कानून बनना एक सराहनीय कदम है, लेकिन असली चुनौती इसके प्रभावी कार्यान्वयन की है। भारत जैसे विशाल और विविधता-भरे देश में जहां डिजिटल साक्षरता अब भी एक चुनौती है, वहां नागरिकों को यह बताना आवश्यक होगा कि उनका डेटा कितना कीमती है और कैसे वे अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही, निजी कंपनियों और विशेष रूप से विदेशी टेक्नोलॉजी दिग्गजों को भी यह स्पष्ट संकेत देना जरूरी है कि भारत में कारोबार करना है तो भारतीय कानूनों और नागरिकों की निजता का सम्मान करना होगा। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह एक मजबूत नियामक तंत्र बनाए, जो पारदर्शी, स्वतंत्र और जवाबदेह हो।
भविष्य की ओर देखते हुए, यह समझना होगा कि हम जिस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें निजता और डेटा सुरक्षा और भी जटिल विषय बनते जाएंगे। स्मार्ट डिवाइस, हेल्थ मॉनिटरिंग गजेट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स हमारे जीवन के हर पहलू को डेटा में बदल रहे हैं। इसलिए अब आवश्यकता है कि हम एक ऐसी नीति और कानून विकसित करें जो केवल आज की समस्याओं का समाधान न करे, बल्कि भविष्य के डिजिटल परिदृश्य को भी ध्यान में रखे। भारत को एक ऐसा मॉडल विकसित करना होगा जो टेक्नोलॉजी और निजता के बीच संतुलन बना सके — और यही एक सशक्त, आत्मनिर्भर और सुरक्षित डिजिटल भारत की बुनियाद बनेगी।
डिजिटल युग में डेटा और निजता अब केवल तकनीकी या कानूनी विषय नहीं रह गए हैं, बल्कि वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गए हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है, वहां निजता का उल्लंघन न केवल संवैधानिक संकट पैदा करता है, बल्कि लोकतंत्र की नींव को भी हिला सकता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इस दिशा में एक साहसी और प्रशंसनीय कदम है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। कानून अपने आप में तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक उसे ईमानदारी, पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता से लागू न किया जाए। इसके लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को मिलकर काम करना होगा।
इस प्रक्रिया में सरकार को चाहिए कि वह सख्त निरीक्षण प्रणाली बनाए, कंपनियों को जवाबदेह बनाए और पारदर्शिता सुनिश्चित करे। निजी कंपनियों को भी समझना होगा कि ग्राहक की जानकारी केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि एक भरोसा है — जिसे बनाए रखना उनके दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए जरूरी है। वहीं नागरिकों को भी अपने अधिकारों को जानने, समझने और उनके उपयोग के लिए तत्पर रहना होगा। जब तक यह तीनों स्तंभ — कानून, उद्योग और नागरिक — एक साथ काम नहीं करते, तब तक डिजिटल निजता केवल एक कानूनी शब्द बना रहेगा। एक समावेशी, सुरक्षित और सशक्त डिजिटल भारत तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक यह जान सके कि उसकी जानकारी उसके नियंत्रण में है और उसे कोई भी ताकत बिना अनुमति के छीन नहीं सकती। यही डिजिटल लोकतंत्र की असली जीत होगी।
(लेखक वरिष्ठ लेखक, पत्रकार, साहित्यकार एवं वैश्विक समूह संपादक, सृजन संसार अंतरराष्ट्रीय पत्रिका समूह)