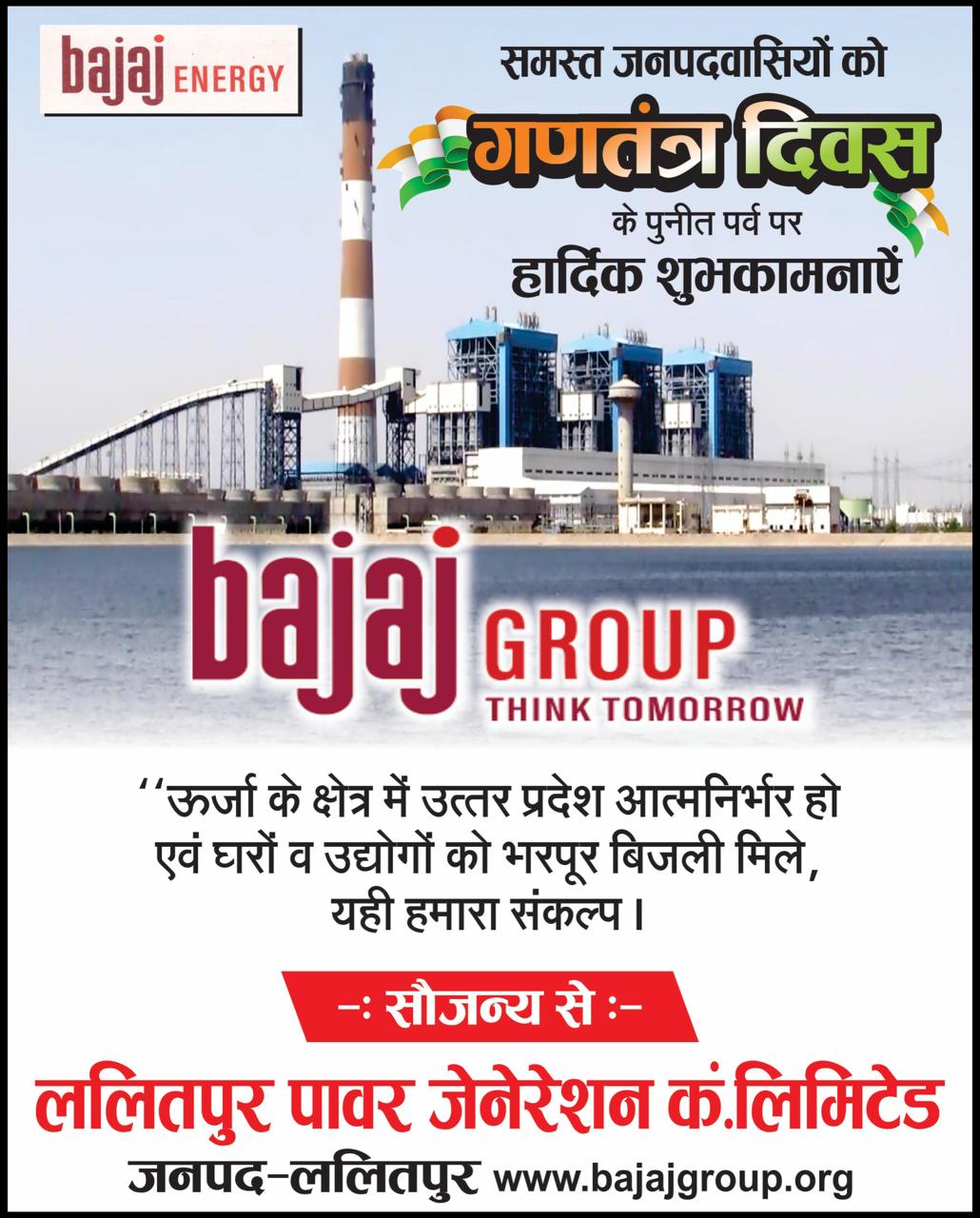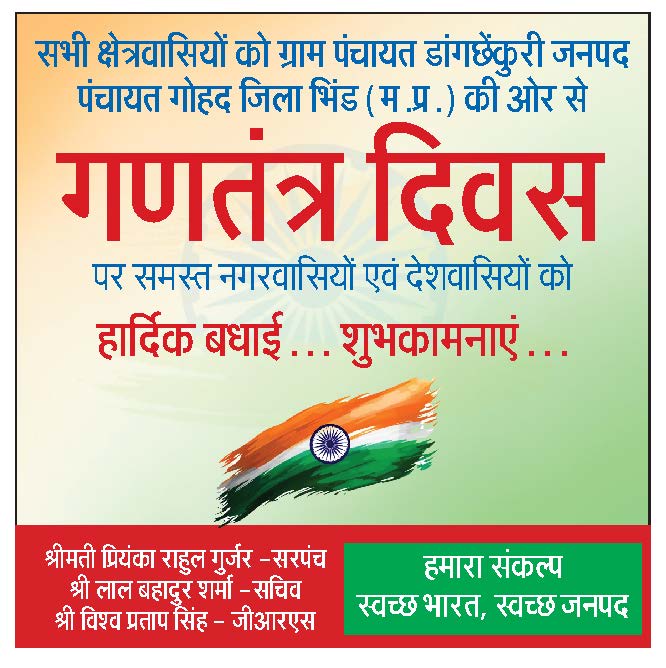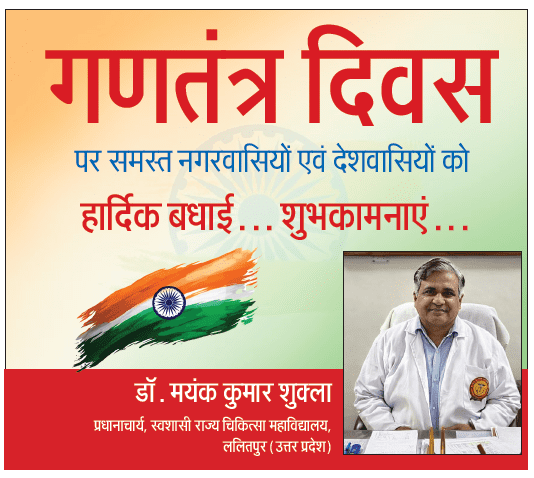2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों में लगभग 189 लोगों की जान गई। लगभग 19 वर्षों तक चले मुकदमे के बाद जब उच्चतम न्यायालय ने सबूतों के अभाव में 12 अभियुक्तों को बरी कर दिया, तो यह न्याय व्यवस्था, जांच एजेंसियों और अभियोजन की निष्क्रियता पर गहरी चोट थी। कमजोर जांच, फॉरेंसिक लापरवाही, जबरन कबूलनामे और गवाहों की सुरक्षा की अनदेखी ने पूरे मामले को खोखला बना दिया। यह घटना हमें बताती है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक, निष्पक्ष और जवाबदेह प्रणाली की आवश्यकता है। वरना जनता का भरोसा केवल व्यवस्था पर से ही नहीं, लोकतंत्र से भी उठ जाएगा।
-प्रियंका सौरभ-
मुंबई में वर्ष 2006 में हुए लोकल ट्रेन धमाके देश के इतिहास की सबसे भयानक आतंकी घटनाओं में से एक थे। सात जगहों पर ट्रेनों में बम विस्फोट कर के 189 लोगों की जान ली गई और लगभग 800 से अधिक लोग घायल हुए। यह हमला केवल मानव शरीरों पर नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की आत्मा पर किया गया था। पूरा देश सन्न रह गया था। भय, आक्रोश और असहायता के बीच एकमात्र आशा थी – न्याय की। परंतु जब लगभग 19 वर्षों बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले के 12 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया, तब एक बार फिर यह प्रश्न गूंजने लगा कि क्या हमारे देश में पीड़ितों को कभी न्याय मिल भी पाता है?
यह निर्णय केवल एक अदालती प्रक्रिया का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उस व्यवस्था की पोल खोलने वाला था जिसमें जांच एजेंसियों की निष्क्रियता, अभियोजन की लापरवाही और राजनीतिक हस्तक्षेप की मिलीजुली साजिश वर्षों से न्याय को घुटनों पर लाने का कार्य कर रही है। किसी भी न्यायालय का कार्य तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक प्रक्रिया के आधार पर निष्पक्ष निर्णय देना होता है। लेकिन जब जांच ही लचर हो, जब सबूत इतने कमजोर हों कि अदालत उन्हें स्वीकार ही न करे, तो फिर न्यायालय भी विवश हो जाता है।
इस मामले में आरोपियों को सज़ा न मिल पाने का दोष न्यायालय पर मढ़ना आसान है, लेकिन वास्तव में जिम्मेदार वे अधिकारी हैं जिन्होंने इस गंभीर आतंकी हमले की जांच को हल्केपन और जल्दबाज़ी से अंजाम दिया। कई आरोपियों के कबूलनामे जबरन करवाए गए, जो कि भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में स्वीकार्य नहीं हैं। विस्फोट स्थलों से फॉरेंसिक साक्ष्य समय पर एकत्रित नहीं किए गए। गवाहों की सुरक्षा को नज़रअंदाज़ किया गया। चार्जशीट्स में विरोधाभासी बातें सामने आईं और अभियोजन पक्ष अदालत में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख सका।
इन सबका परिणाम यह हुआ कि वे लोग जो सालों से दोषियों को सज़ा दिलाने की उम्मीद में अदालतों के चक्कर काट रहे थे, उन्हें अंत में निराशा ही हाथ लगी। क्या इस देश में किसी आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या पीड़ित परिवारों की आंखों के आँसू, उनकी टूटती उम्मीदें और उनके जीवन की असुरक्षा हमारी व्यवस्था को झकझोरने के लिए काफी नहीं?
यह कोई पहला मामला नहीं है जहां न्याय व्यवस्था ने पीड़ितों को न्याय दिलाने में असफलता दिखाई हो। भोपाल गैस त्रासदी, हाशिमपुरा नरसंहार, 1984 सिख दंगे, और निठारी हत्याकांड – यह सभी उदाहरण हैं जहां या तो दोषी छूट गए या न्याय मिलने में इतनी देर हुई कि उसका कोई अर्थ ही नहीं बचा। यह सबूत हैं कि हमारी न्यायिक प्रणाली में समय, साक्ष्य और सत्य – तीनों की कमी होती जा रही है।
न्याय केवल अदालत में फैसले देने की प्रक्रिया नहीं है, वह समाज के उस विश्वास की रीढ़ है जो शासन और प्रशासन पर टिका होता है। यदि बार-बार अपराधी बच निकलें, यदि आतंकवादी छूट जाएं, और यदि पीड़ित सालों अदालतों की सीढ़ियां चढ़ते रहें तो वह विश्वास ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है।
मुंबई ट्रेन धमाके की जांच जिस प्रकार से की गई, वह बताता है कि हमारी जांच एजेंसियां न केवल तकनीकी रूप से कमजोर हैं, बल्कि वे राजनीतिक दबाव में काम करने के लिए अभिशप्त भी हैं। भारत में जांच का ढांचा ब्रिटिशकालीन मानसिकता पर आधारित है, जिसमें अपराधी को पकड़ने से ज़्यादा उसे “दिखाने” पर ज़ोर होता है। और जब मामला आतंकवाद से जुड़ा हो, तो कई बार बेकसूरों को पकड़ कर जनता के गुस्से को शांत करने की कोशिश की जाती है। इससे असली अपराधी कभी पकड़ा ही नहीं जाता, और सारा केस अदालत में दम तोड़ देता है।
इस मामले में भी कई ऐसे पहलू हैं जो चिंता पैदा करते हैं। जैसे – जांच में देरी, सबूतों का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह न होना, अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य न होना, और गवाहों का मुकर जाना। इन सब कमियों के बावजूद यदि हम न्याय की उम्मीद करें, तो यह केवल छलावा होगा।
क्या न्यायपालिका को केवल मौन दर्शक बने रहना चाहिए? क्या उसका कोई दायित्व नहीं कि वह जांच की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए? जब अदालतों ने कई अन्य मामलों में विशेष जांच दल (SIT) गठित किए हैं, तो फिर इस गंभीर मामले में क्यों नहीं? न्यायिक सक्रियता केवल राजनैतिक मामलों या नागरिक अधिकारों तक ही सीमित क्यों?
वास्तव में न्याय प्रणाली को समयबद्ध, वैज्ञानिक और जवाबदेह बनाने के लिए एक सम्पूर्ण सुधार की आवश्यकता है। सबसे पहले तो अभियोजन विभाग को पुलिस से अलग कर स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अभियोजन किसी राजनीतिक दबाव या पुलिस की एकतरफा जांच का हिस्सा नहीं बनेगा।
दूसरे, गवाह सुरक्षा कानून को प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। आतंकवाद जैसे मामलों में गवाहों को धमकाना बहुत आम है, जिससे वे अदालत में बयान बदल देते हैं। तीसरे, जांच एजेंसियों को तकनीकी प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण दिए जाने चाहिए ताकि वे डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों को प्रभावी रूप से इकट्ठा कर सकें।
चौथे, फास्ट ट्रैक अदालतें बनाकर ऐसे मामलों की सुनवाई समयबद्ध तरीके से करनी चाहिए, ताकि पीड़ितों को 19 साल तक न्याय की प्रतीक्षा न करनी पड़े। और पांचवां, यदि कोई जांच एजेंसी जानबूझकर कमजोर चार्जशीट बनाती है, तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पक्ष है – मीडिया की भूमिका। मीडिया को भी आत्ममंथन करना होगा। जब कोई मामला अदालत में हो, तब मीडिया द्वारा किसी को दोषी या निर्दोष घोषित कर देना, न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मीडिया ट्रायल से गवाहों पर दबाव बनता है और जनता का पूर्वग्रह उभरता है। यह भी कारण है कि न्याय अपने नैतिक स्वरूप से दूर होता जा रहा है।
आख़िर में यही कहा जा सकता है कि न्याय केवल कागज़ी प्रक्रिया नहीं है, वह एक जीवंत विश्वास है, जो प्रत्येक नागरिक के मन में इस सोच के साथ पलता है कि कोई उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता। जब यह विश्वास टूटता है, तब देश की आत्मा घायल होती है।
मुंबई ट्रेन धमाकों के पीड़ितों के साथ जो हुआ, वह केवल एक अदालती मामला नहीं है – वह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि यदि अब भी हमने अपनी व्यवस्था को नहीं सुधारा, तो अगली बार फिर कोई धमाका होगा, फिर निर्दोष मारे जाएंगे, फिर कोई माँ न्याय की भीख मांगेगी, और फिर कोई अदालत कहेगी – साक्ष्य नहीं मिले।
इस बार अगर हम नहीं जागे, तो इतिहास बार-बार यह प्रश्न पूछेगा – क्या भारत में न्याय केवल सुविधा भर है?