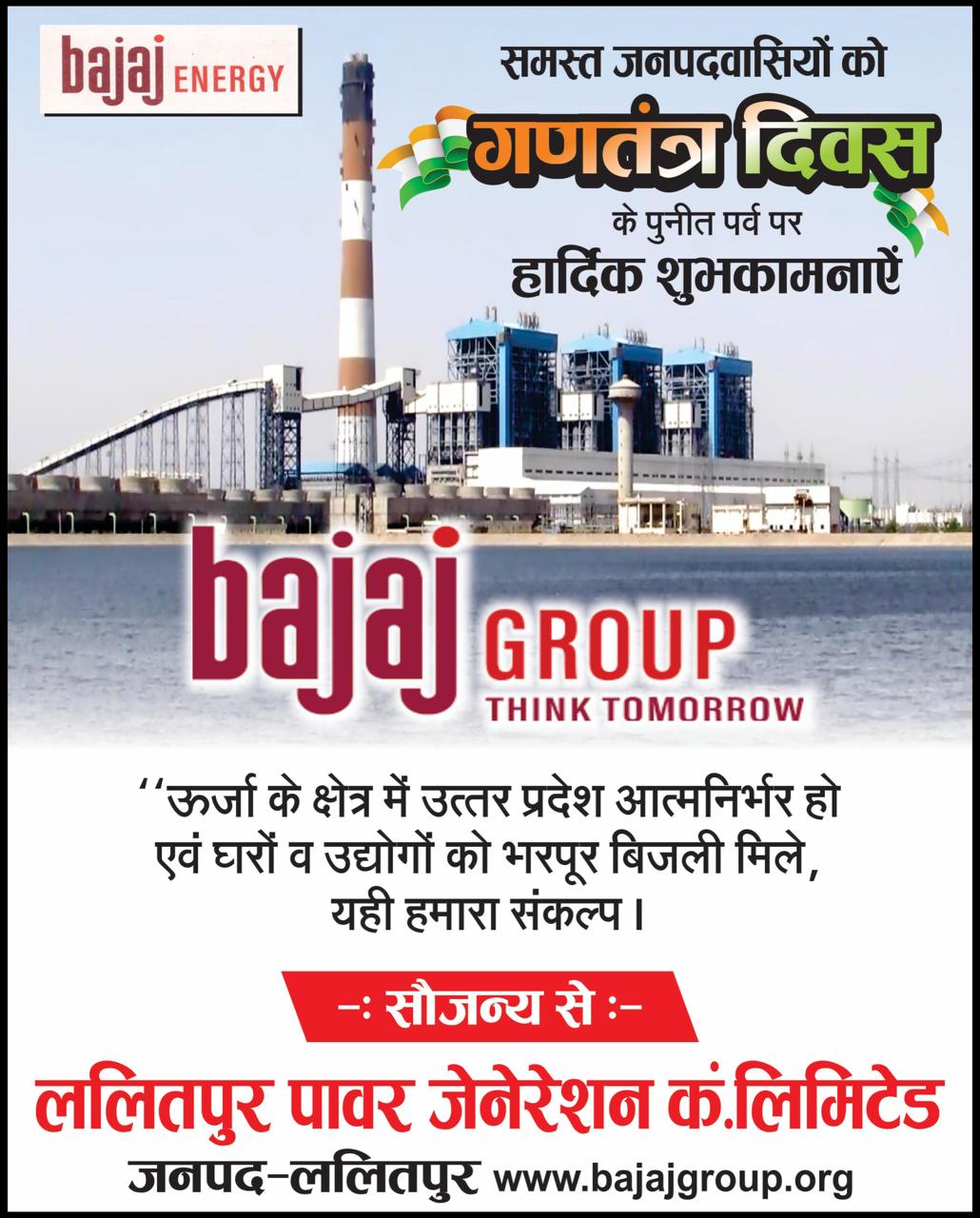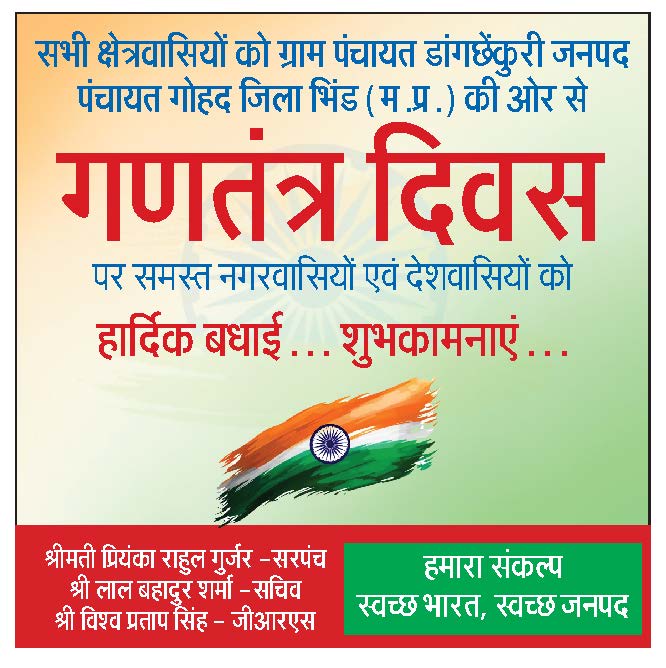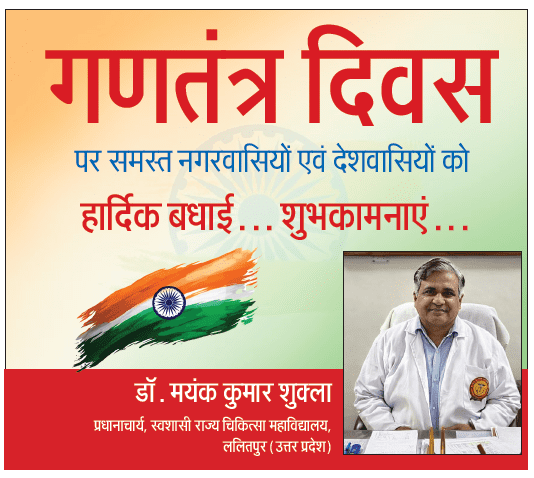– प्रकाश गवांदे –
भारत में समाजवादी विचारधारा को एक आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने तथा उसे प्रभावी रीति से प्रचारित करने वाले चिंतकों में डॉ. राममनोहर लोहिया का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। वे एक गांधीवादी चिंतक, राजनीतिक इतिहासकार, अर्थशास्त्री, दार्शनिक तथा विख्यात लेखक थे। जीवन के प्रायः सभी पक्षों पर उन्होंने गहन चिंतन किया तथा भारतीय परिस्थितियों में इसे व्यावहारिक बनाने के उपायों का सफलतापूर्वक आजीवन अन्वेषण किया।
डॉ. लोहिया गांधीवादी थे लेकिन उनके विचारों में उग्रता थी। वे क्रांतिकारी थे, लेकिन उनके विचारों में असाधारण रचनात्मकता थी। वे एक विख्यात एवं सक्रिय राजनीतिज्ञ थे, किन्तु उनकी शैली एवं कार्यों में सिद्धांतों के प्रति असाधारण लगाव था। उन्होंने समाजवाद के महान उद्देश्यों की भारतीय संदर्भों में व्याख्या की तथा उसे व्यावहारिक बनाया।
डॉ. राममनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद (वर्तमान – अम्बेडकर नगर) के अकबरपुर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिताजी गांधीजी के अनुयायी थे। जब वे गांधीजी से मिलने जाते तो राममनोहर को भी अपने साथ ले जाया करते थे। इसके कारण गांधीजी के विराट व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर हुआ। पिताजी के साथ 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए।
डॉ. लोहिया के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार
डॉ. लोहिया के विचारों पर कार्ल मार्क्स एवं महात्मा गांधी — दोनों के विचारों का असाधारण प्रभाव परिलक्षित होता है। उन्होंने इनमें अद्भुत समन्वय स्थापित किया तथा इनके श्रेष्ठतम तत्वों को समाहित करते हुए नवीन विचारों का विकास किया।
जाति और वर्गों में संघर्ष की धारणा
डॉ. लोहिया के अनुसार इतिहास में जाति और वर्गों में संघर्ष होता रहता है, और इसी से इतिहास को गति मिलती है। जातियों का रूप सुनिश्चित होता है, किन्तु वर्गों की आंतरिक रचना शिथिल होती है। इन दोनों के बीच घड़ी के पेंडुलम के समान आंतरिक क्रियाएं होती रहती हैं — इन्हीं से इतिहास को गति मिलती है।
डॉ. लोहिया के अनुसार जातियों में सामान्यतः गतिहीनता और निष्क्रियता पाई जाती है, जबकि वर्ग सामाजिक गतिशीलता की प्रचंड शक्तियों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्ग संगठित होकर जातियों का रूप धारण कर लेते हैं, और जातियाँ वर्गों में परिणत हो जाती हैं। मानव जाति का अब तक का इतिहास जातियों और वर्गों के बीच आंतरिक संघर्षों का इतिहास है।
एशियाई समाजवाद का विचार
डॉ. लोहिया का विचार था कि एशियाई राष्ट्रों की अपनी विशिष्ट समस्याएँ हैं, जिन्हें एशियाई तरीकों से ही हल किया जाना चाहिए। उनका कथन था कि एशिया में जहाँ आर्थिक समस्याएँ मुँह बाए खड़ी हैं, वहाँ पश्चिमी ढंग का समाजवादी प्रजातंत्र उपयोगी नहीं हो सकता।
एशिया के लोग रोटी के लिए अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों को बेचने के लिए सरलता से तैयार हो जाएँगे। परंपरागत सोच के अनुसार रोटी की समस्या के समाधान हेतु हमें पूँजीवादी अथवा साम्यवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना ही अनिवार्य दिखाई देती है, किन्तु दोनों की अर्थव्यवस्था एक जैसी ही है। अंतर केवल इतना है कि पूँजीवाद यदि निजी संपत्ति को प्रोत्साहित करता है तो साम्यवाद सार्वजनिक संपत्ति को। पूँजी और सत्ता का केंद्रीकरण दोनों में समान रूप से है।
डॉ. लोहिया मानते थे कि यूरोप का मशीनी समाजवाद एशिया के देशों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ गरीबी अधिक है। उनका कथन था कि परंपरागत आर्थिक विकेंद्रीकरण से एशिया की गरीबी दूर नहीं हो सकती। यहाँ बड़ी मशीनों के स्थान पर गांधीजी के विचारों का अनुसरण करते हुए छोटी-छोटी मशीनों का प्रयोग करना चाहिए।
इस प्रकार, कुटीर उद्योगों में धन भी कम लगेगा तथा बेरोज़गारी भी घटेगी। डॉ. लोहिया सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करने के पक्ष में थे। वे पाश्चात्य समाजवाद को संवैधानिक एवं विकासवादी निरूपित करते हुए उसे एशिया के लिए अनुपयोगी मानते थे।
धर्म एवं राजनीति का समन्वय
डॉ. लोहिया कहा करते थे कि राजनीति के बिना धर्म निष्प्राण हो जाता है तथा धर्म के बिना राजनीति कलही बन जाती है। वे धर्म को दीर्घकालीन राजनीति तथा राजनीति को अल्पकालीन धर्म कहते थे।
सप्त क्रांति का सिद्धांत
डॉ. लोहिया अनुभव करते थे कि किसी एकजुट कार्यक्रम के अभाव में भारत में प्रतिपक्षी दल आपस में लड़ते रहते हैं। इसका लाभ सत्तारूढ़ दल को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। उन्होंने समाजवाद के सार्वभौम सात सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने की बात कही थी —
स्त्री-पुरुष समानता की स्वीकृति
जाति एवं जन्म-आधारित असमानता की समाप्ति
रंगभेद पर आधारित असमानता की समाप्ति
विदेशियों द्वारा दमन की समाप्ति तथा विश्व सरकार का निर्माण
व्यक्तिगत संपत्ति पर आधारित आर्थिक असमानताओं का विरोध तथा उत्पादन में योजनाबद्ध वृद्धि
व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण का विरोध
युद्ध के शस्त्रों का विरोध तथा सविनय अवज्ञा सिद्धांत की स्वीकृति
विश्व संसद का समर्थन
डॉ. लोहिया ने वैश्विक समस्याओं को सुलझाने के लिए विश्व संसद का समर्थन किया था। वे चाहते थे कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई विश्व पंचायत की स्थापना होनी चाहिए। इस पंचायत को समस्त राज्यों के युद्ध बजट का एक-चौथाई अथवा पाँचवाँ हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। वे मानते थे कि सत्याग्रह के द्वारा भी विश्व पंचायत की स्थापना संभव है।
निरंकुश शासन का विरोध
डॉ. लोहिया को निरंकुश शासन स्वीकार्य नहीं था। वे आर्थिक एवं राजनीतिक विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। वे सत्ता को राज्य, प्रांत, जिला तथा ग्राम स्तर पर बाँटकर ‘चौखंभा राज्य’ की स्थापना करना चाहते थे।
भारत-विभाजन पर लोहिया के विचार
डॉ. लोहिया ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “Guilty Men and India’s Partition” (भारत विभाजन के गुनहगार) में उस समय की कई घटनाओं और परिस्थितियों का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के उस दौर की सच्चाई को उजागर किया, जिसे उन्होंने स्वयं अपनी आँखों से देखा था।
निष्कर्ष
डॉ. राममनोहर लोहिया पर मार्क्सवाद एवं गांधीवाद — दोनों का गहरा प्रभाव था। उन्होंने अपनी निराली शैली में इन दोनों महान विचारधाराओं के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या की तथा उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया।
मुक्त चिंतन, निर्भीकता, मौलिकता और अनूठा समन्वयवाद उनके व्यक्तित्व की सहज विशेषताएँ थीं। इन्हीं के आधार पर उन्होंने एक नई समाजवादी व्यवस्था का स्वप्न देखा था। उन्होंने आधुनिक सभ्यता को स्वीकार किया, किन्तु उसमें सुधार करते हुए उसे और अधिक मानवीय बनाने का प्रयास किया।
डॉ. लोहिया शांतिवादी होते हुए भी प्रबल विद्रोही और महान क्रांतिकारी थे — और आधुनिक भारत को आज भी ऐसे ही समाजवादी चिंतकों की आवश्यकता है।