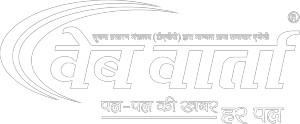– संजय गोस्वामी –
विश्व ओज़ोन दिवस 2025, हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिवस पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक पराबैंगनी (यूवी) विकिरण से बचाने में ओज़ोन परत के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का दिन है।
विश्व ओज़ोन दिवस 2025 का विषय विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की उपलब्धियों और निरंतर महत्व को उजागर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की एक पहल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का स्मरण और ओज़ोन परत की सुरक्षा के प्रयासों को बढ़ावा देना होगा। यह दिन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने और मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिक तंत्र और ग्रह की सुरक्षा में ओज़ोन परत की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है।
ओजोन परत क्षय एक गंभीर चुनौती
ओजोन परत समुद्र सतह से 60 कि.मी. की ऊंचाई तक विविध सांद्रता वाली परतों में पाई जाती है। ओजोन गैस ऊपर वायुमण्डल में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत बनाते हैं! ओजोन लेयर ऑक्सीजन गैस का ही एक रूप होता है! जब ऑक्सीजन के तीन परमाणु एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो ओजोन का निर्माण करते हैं!
वायुमण्डल में ओजोन गैस का एक छाता सा आवरण पाया जाता है जिसे ओजोन परत या ओजोन मण्डल कह सकते हैं। वायुमण्डल की ऊंचाई 16 से 29 किलोमीटर तक मानी जाती है। तापक्रम तथा वायुमण्डल के कारण वायुमण्डल का परिवर्तन मण्डल, ओजोन मण्डल, समताप मण्डल तथा मध्य मण्डल उर्ध्वाकार विभाजन किया गया है। इसमें प्रमुख है ओजोन परत मण्डल जो ओजोन परत के नाम से जाना जाता है।
यह परत पृथ्वी के धरातल से 20–30 कि.मी. की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन परत ऑक्सीजन के तीन परमाणु से मिलकर बनती है। यह परत वायुमण्डल में बहुत कम है। यह परत धरती के निकट होती तो इससे मानव के शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता जिससे मनुष्य अनेक रोगों से पीड़ित हो जाता।
जहां यह परत धरती के लिए हानिकारक है, वहीं यह परत वायुमण्डल में ऊपर होने से मनुष्यों के लिए लाभदायक है। सूरज से निकलने वाली सबसे हानिकारक गैस है पैराबैंगनी किरण! पैराबैंगनी किरणें न ही सिर्फ मनुष्य बल्कि जीव-जंतुओं और वनस्पतियों के लिए अत्यंत हानिकारक हैं।
सूरज की नुकसानदेह किरणों से बचाने वाली हमारी जीवन रक्षक परत ओजोन बेहद पतली हो चुकी है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से धरती को बचाने वाली ओजोन परत में छेद हो चुका है। जब आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में इतना विशाल छिद्र देखा गया है, वैज्ञानिकों को कई तरह की चिंताएं सता रही हैं।
ओजोन परत का अध्ययन करने वाले जेट प्रॉपल्सन लैबोरेटरी, कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने ताजा रिपोर्ट तैयार की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सैटेलाइट्स से मिली तस्वीरों के आधार पर रिपोर्ट कहती है कि ओजोन परत पर उत्तरी अमेरिका के आकार जितना बड़ा छेद हो चुका है। इसका आकार 2.5 वर्ग किलोमीटर आंका गया है। वैज्ञानिक 1980 से ओजोन परत में हो रहे छिद्र का अध्ययन कर रहे हैं।
हर साल ग्लोब के सबसे निचले हिस्से अंटार्कटिका में जाकर ओजोन परत पर नजर रखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों को आशंका है कि ओजोन परत का छेद फैलकर दक्षिणी अमेरिका तक पहुंच सकता है। ऐसी परिस्थितियों में ब्राजील, चिली और पेरू समेत कई देशों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा।
सूरज की पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियां महामारी का रूप ले सकती हैं। यह सब ग्रीन हाऊस गैसों से है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ है। इनमें सबसे खतरनाक क्लोरो-फ्लोरो कार्बन गैस है जो ओजोन के परमाणुओं को कम कर रहा है। इसकी वजह से हर साल ओजोन परत 4 प्रतिशत की दर से कम हो रही हैं।
यदि ओजोन के नुकसान की यही गति रही तो अगले 50 से 60 साल में ओजोन का 15 से 20 प्रतिशत भाग नष्ट हो जाएगा। इससे पराबैंगनी किरणों के पृथ्वी के धरातल पर पड़ने से तेज धूप होगी जिससे जीव-जंतुओं में जल की कमी होगी और वे गर्मी से झुलस जाएंगे।
नाइट्रस आक्साइड एक हरितगृह गैस है जो वैश्विक तपन के साथ-साथ समतापमंडलीय ओजोन परत की क्षय के लिए भी उत्तरदायी है। रक्षा कवच के रूप में ओजोन परत सूर्य की हानिकारक परा-बैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है।
धान की खेती के विस्तार के फलस्वरूप मीथेन गैस की उत्सर्जन की दर में बढ़ोत्तरी हुई है। मीथेन भी नाइट्रस आक्साइड की तरह हरितगृह गैस है जो वैश्विक तपन के लिए उत्तरदायी है।
ओजोन परत की बिरलता न केवल तापमान वृद्धि हो रही है बल्कि जलवायु परिवर्तन का यह एक बड़ा कारण है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम जैव-भू-जैव रासायनिक चक्र में परिवर्तन होना है।
एक तरफ मानव जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है वहीं दूसरी तरफ हिमखण्ड पिघलने से भूक्षेत्र में कमी आ रही है। आने वाले समय में यह स्थिति अराजकता और अव्यवस्था का परिचायक दिखलाई पड़ रही है।
ओजोन परत में विरलता से वह अमलीय वर्षा और घने कुहरे का प्रकोप दुनिया झेल रही है। वहीँ दूसरी तरफ इस विखण्डन के नाते पराबैंगनी बीटा किरणों की अधिकता से न केवल पशु, पौधे बल्कि मानव भी बुरी तरह से दुष्प्रभावित है।
विभिन्न प्रकार के होने वाले चर्म रोग, कैंसर रोग, मोतियाबिंद, चमड़ियों में झुर्री पड़ना, त्वचा की कोशिकाओं में टूट-फूट होना इत्यादि संकट से आज यह जगत दो चार हो रहा है। समय रहते इसके समझ लें और ठीक करने की अत्यन्त आवश्यकता है। वरना आने वाली पीढ़ी इस मार को सहने को अक्षम होगी।
न्यूजीलैण्ड के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर आकाश में ओजोन परत का छिद्र बढ़कर काफी बड़े आकार का होकर दक्षिणी अमेरिका के एक शहर तक फैल गया है। अंटार्कटिका पोल के ऊपर की परत में छेद हो गया है जो लगभग यूरोप के भौगोलिक आकार का है।
ओजोन परत क्षरण का प्रमुख कारण है समताप मण्डल में अत्यधिक प्रदूषण का होना। सूर्य के प्रकाश में हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं परंतु जब पराबैंगनी किरणों के कारण अत्यधिक धूप होगी तो जल को वह सोख लेगी और पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और वे सूख जाएंगे।
पराबैंगनी किरणों के कारण अनेक रोग उत्पन्न होंगे, हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति या क्षमता धीरे-धीरे कम हो जाएगी। पराबैंगनी किरणों के कारण हमारा शरीर तो झुलस ही जाएगा, अनेक प्रकार के चर्म रोग भी उत्पन्न होंगे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस गति से ओजोन परत का क्षय हो रहा है।
मनुष्यों के अनेक क्रियाकलापों से उत्पन्न क्लोरो फ्लोरो कार्बन (CFC) यौगिक हैलोजन्स (क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन) तथा नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा वायुमण्डल में अधिक है। इन सभी हानिकारक गैसों के कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है।
इससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ रही हैं। ओजोन परत के क्षरण का सबसे बड़ा कारण मनुष्यों द्वारा उत्पन्न किया गया क्लोरो फ्लोरो कार्बन यौगिक है, रेफ्रीजरेटरों और ए.सी. जैसे विद्युत उपकरणों और प्लास्टिक के फोम बनाते समय होती है।
ओजोन परत के क्षरण से अधिक हानि है तालाब, झील व नदियों का सूख जाना। अत्यधिक गर्मी के बढ़ने के कारण झील, तालाब और नदियों का पानी सूख जाएगा तथा जीव-जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ जाएगा।
प्रत्येक वर्ष ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवों पर ग्लेशियर पिघलने की गति बढ़ती जा रही है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण वैश्विक तपन है जो हरितगृह प्रभाव का परिणाम है। वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी से टकराकर लौटने वाली सूर्य की किरणों को वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें अवशोषित कर लेती हैं, जिसके परिणामस्वरुप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, को हरितगृह प्रभाव के नाम से जाना जाता है।
वह गैसें जो हरितगृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं, को हरितगृह गैस के नाम से जाना जाता है। कार्बन डाईऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्षोभमण्डलीय ओजोन मुख्य हरितगृह गैसें हैं जो हरितगृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं।
विभिन्न कारणों से वातावरण में इनकी निरन्तर बढ़ती मात्रा से वैश्विक जलवायु परिवर्तन का खतरा दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। फलस्वरूप समुद्र के तल में असामान्य रूप से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों व छोटे द्वीपों के लिए चेतावनी है, क्योंकि इससे उनके अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लग रहा है।
सामान्यतः समुद्र का उपयोग जलमार्ग के रूप में किया जाता है। इससे इसके किनारों पर बंदरगाह का विकास होता है तथा स्थानीय शहरों का विकास व रोजगार का सृजन भी होता है। परन्तु समुद्र तल में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती रही तो छोटे द्वीप व समुद्र सीमा पर बसे व्यावसायिक शहर जलमग्न हो सकते हैं। इसके फलस्वरूप एक बड़ी आबादी का पलायन, कृषि उत्पादन में कमी, स्वच्छ जल उपलब्धता का संकट एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव इसकी भयावहता को प्रकट करती है।
प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन तथा अनुचित मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंच रही है। इसके अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं परन्तु भविष्य की कल्पना कर हम इसे संरक्षित व और अधिक लाभकारी बनाने का प्रयास कर सकते हैं।
वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट की समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी है तथा इसमें अधिकतम प्रतिशत घरेलु व व्यवसायिक संस्थानों से निकला प्लास्टिक अपशिष्ट है जो कि नॉन-बायोडिग्रेडेबल होता है जो अनेक तरह के पर्यावरणीय प्रदूषणों का कारक होता है।
जन सामान्य को पॉलीथिन अपशिष्ट से पर्यावरण पर पड़ने वाले दीर्घकालिक दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तथा पॉलीथीन के सीमित या उपयोग न करने के बारे में औद्योगिक इकाइयों द्वारा भी विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है जिसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है।
भीषण बाढ़ व तूफान : जब अधिक गर्मी बढ़ेगी तो हिमालय एवं अन्य बर्फीले क्षेत्रों की बर्फ पिघलेगी और समुद्र में जल की मात्रा अधिक हो जाएगी तथा भीषण बाढ़ के साथ तूफानों के आने की संभावना भी है।
ओजोन परत का नाश करने में सबसे बड़ा योगदान हम मनुष्यों का ही है! हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ ऐसे उपकरणों का उपयोग करते हैं जो कि बहुत ही हानिकारक गैसे क्लोरो फ्लोरो कार्बन (CFC) यौगिक हैलोजन्स तथा नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। इस ज्ञान से ओजोन परत क्षति, औद्योगिक प्रदूषण, सामाजिक चेतना के अभाव आदि कई-कई घटकों पर प्रभावी नियंत्रण से प्राकृतिक संतुलन की पुनर्स्थापना की जा सकती है।
पर्यावरण की रक्षा के लिए ओजोन परत क्षय एक गंभीर समस्या है। समय रहते संभलना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने पृथ्वी की ओजोन परत को हुए नुकसान को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से हुई संधि के परिणामस्वरूप दुनिया भर की सरकारें उन रसायनों का उपयोग खत्म कर रही हैं, जिनसे ओजोन परत का क्षय हुआ है। उनकी जगह सुरक्षित विकल्प अपनाए जा रहे हैं जिससे हमारी समूची प्रकृति (जल, थल तथा वायुमंडल) का बचाव हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप लाखों लोगों के लिए पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से त्वचा कैंसर का जोखिम कम होता है।
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं। इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।)